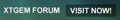



hatha pradipika
भगवान शिव को नमस्कार
नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने । निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायण: ।। 1 ।।
भावार्थ :- जिस प्रकार शेषनाग को वन पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी का आधार माना जाता है । ठीक उसी प्रकार कुण्डलिनी शक्ति को सभी योग व तन्त्रों का आधार माना जाता है ।
समाधि वर्णन
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधिक्रममुत्तमम् । मृत्युध्नं च सुखोपायं ब्रह्मानन्दकरं परम् ।। 2 ।।
भावार्थ :- अब इसके बाद मैं मृत्यु का नाश करने वाली, सुख प्रदान करवाने वाली व ब्रह्मानन्द का अनुभव करवाने वाली समाधि की उत्तम विधि का उपदेश करूँगा ।
राजयोग: समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी । अमरत्वं लयस्तत्त्वं शून्याशून्यं परं पदम् ।। 3 ।। अमनस्कं तथा द्वैतं निरालम्बं निरञ्जनम् । जीवनमुक्तिकश्च सहजा तुर्या चेत्येकवाचका: ।। 4 ।।
भावार्थ :- राजयोग, समाधि, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, अमरत्व, लय, तत्त्व, शून्याशून्य, परमपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालम्बन, निरञ्जन, जीवन मुक्ति, सहजा अवस्था तथा तुर्या अवस्था इन सभी के सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता हैं । दूसरे अर्थ में हम इनको एक दूसरे के पर्यायवाची भी कह सकते हैं । विशेष :- जहाँ पर भी उपर्युक्त शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा । उसका अर्थ समाधि ही माना जाएगा । इन सभी शब्दों का प्रयोग समाधि के लिए ही किया जाता है ।
योग अथवा समाधि की परिभाषा
सलिले सैन्धवं यद्वत् साम्यं भजति योगत: । तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ।। 5 ।।
भावार्थ :- जिस प्रकार पानी में नमक डालने से वह नमक पानी के साथ घुलकर पानी के समान ही हो जाता है । ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन की एकरूपता अर्थात् आत्मा और मन के आपस में मिलने को समाधि की अवस्था कहते हैं । विशेष :- हठयोग के अनुसार इस श्लोक को योग अथवा समाधि की परिभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है । जिस प्रकार योगश्चितवृत्ति निरोध: को योगदर्शन के अनुसार व योग: कर्मसु कौशलम् को गीता के अनुसार योग की परिभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है । ठीक उसी प्रकार हठयोग के अनुसार इस श्लोक को योग की परिभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है ।
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते ।। 6 ।।
भावार्थ :- प्राणों की गति मन्द होने से मन भी गतिविहीन अर्थात् स्थिर हो जाता है । इन दोनों ( प्राण व मन ) की एकरूपता ( एक होने ) को ही समाधि कहते हैं ।
तत्समं च द्वयोरैक्यं जीवात्मपरमात्मनो: । प्रनष्टसर्वसङ्कल्प: समाधि: सोऽभिधीयते ।। 7 ।।
भावार्थ :- जीवात्मा और परमात्मा की एकरूपता ( एक होने ) होने से साधक के सभी संकल्प अर्थात् सभी इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं । इस अवस्था को भी समाधि कहते हैं ।
गुरु का महत्त्व
राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः । ज्ञानं मुक्ति: स्थिति: सिद्धिर्गुरूवाक्येन लभ्यते ।। 8 ।।
भावार्थ :- राजयोग की उपयोगिता को कोई विरला ही जान पाता होगा । इसका ज्ञान, मुक्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना व सिद्धि की प्राप्ति आदि का लाभ गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होता है ।
दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् । दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो: करुणां विना ।। 9 ।।
भावार्थ :- उत्तम गुरु की विशेष कृपा के बिना विषयों अर्थात् आसक्ति का त्याग, यथार्थ ज्ञान का मिलना व सहजावस्था अर्थात् समाधि की अवस्था का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है ।
विविधैरासनै: कुम्भैर्विचित्रै: करणैरपि । प्रबुद्धायां महाशक्तौ प्राण: शून्ये प्रलीयते ।। 10 ।।
भावार्थ :- अनेक प्रकार के आसनों, कुम्भकों ( प्राणायाम ) व अनेक प्रकार की योग साधनाओं का अभ्यास करने से साधक कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है । जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी में लीन ( मिल जाना ) हो जाता है ।
उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनि: शेषकर्मण: । योगिन: सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते ।। 11 ।।
भावार्थ :- कुण्डलिनी शक्ति के उत्पन्न होने अर्थात् जागृत होने व सभी कर्मों का त्याग ( सभी सकाम कर्म अर्थात् जो कर्म बन्धन का कारण बनते हैं ) करने से योगी की समाधि अपने आप ही लग जाती है । उसके लिए उसे किसी अन्य प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती ।
।। सुषुम्नावाहिनि प्राणे शून्ये विशति मानसे । तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित् ।। 12 ।।
भावार्थ :- साधक का प्राण जब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लेता है तो उसका मन भी शून्यभाव ( मन का विचारों से रहित होना ) को प्राप्त हो जाता है । तब साधक सभी प्रकार के क्रियाकलापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है ।
अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जित: । पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम् ।। 13 ।।
भावार्थ :- जिस अमर योगी ने इस सारे जगत को अपने वश में रखने वाली मृत्यु को भी जीत लिया है । ऐसे श्रेष्ठ योगी को नमस्कार ।
चित्ते समत्वमापन्ने वायौ व्रजति मध्यमे । तदामरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते ।। 14 ।।
भावार्थ :- साधक का चित्त समभाव ( समता ) को प्राप्त होने पर उसका प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लेता है । इस प्रकार प्राणवायु के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद ही साधक की अमरोली, वज्रोली व सहजोली क्रियाएँ सिद्ध होती है ।
मोक्ष प्राप्ति
ज्ञानं कुतो मनसि सम्भवतीह तावत् प्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न यावत् । प्राणो मनो द्वयमिदं विलयं नयोद्यो मोक्षं स गच्छति नरो न कथञ्चिदन्य: ।। 15 ।।
भावार्थ :- जब तक साधक के प्राण का निरन्तर प्रवाह होता रहता है तब तक उसका मन भी शान्त नहीं होता और मन के शान्त न होने से उसे यथार्थ ज्ञान ( वास्तविक ज्ञान ) की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? जो साधक अपने प्राणों व मन का पूरी तरह से निरोध कर लेता है । उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है । अन्य किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है ।
ज्ञात्वा सुषुम्ना सम्भेदं कृत्वा वायुं च मध्यगम् । स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरण्ध्रे निरोधयेत् ।। 16 ।।
भावार्थ :- साधक को सदा सुन्दर स्थान पर बैठकर सुषुम्ना नाड़ी का अच्छी प्रकार से भेदन करके प्राणवायु को सुषुम्ना नाड़ी के अन्दर प्रवेश करवाकर ब्रह्मरन्ध्र में उसका निरोध करना चाहिए ।
सूर्याचन्द्रमसौ धत्त: कालं रात्रिन्दिवात्मकम् । भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेतदुदाहृतम् ।। 17 ।।
भावार्थ :- दिन और रात को सूर्य और चन्द्रमा धारण ( सूर्य और चन्द्रमा से ही दिन व रात का आभास होता है ) करते हैं । सुषुम्ना नाड़ी उस काल ( दिन व रात के समय ) को भोगने वाली है । इसे अत्यन्त गुप्त रहस्य कहा गया है ।
सभी बहत्तर हजार ( 72000 ) नाड़ियाँ में सुषुम्ना की महत्ता
द्वासप्तति सहस्त्राणि नाडीद्वाराणि पञ्जरे । सुषुम्ना शाम्भवी शक्ति: शेषास्त्वेव निरर्थका: ।। 18 ।।
भावार्थ :- इस मानव शरीर में कुल बहत्तर हजार ( 72000 ) नाड़ियाँ है । इनमें से सुषुम्ना नाड़ी ही सबसे प्रमुख है जिसे शाम्भवी शक्ति भी कहते हैं । बाकी की सभी नाड़ियों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । वह एक प्रकार से निरर्थक अर्थात् महत्त्वहीन हैं ।
वायु: परिचितो यस्मादग्निना सह कुण्डलीम् । बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशेदनिरोधत: ।। 19 ।। सुषुम्नावाहिनि प्राणे सिद्घयत्येव मनोन्मनी । अन्यथात्वितराभ्यासा: प्रयासायैव योगिनाम् ।। 20 ।।
भावार्थ :- चूँकि अच्छे अभ्यास से भली प्रकार से वश में किया हुआ प्राण अग्नि तत्त्व के साथ मिलकर कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करके बिना किसी प्रकार की बाधा के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है । इस प्रकार जब साधक का प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है तभी मनोन्मनी अवस्था अर्थात् समाधि की सिद्धि होती है । इसके अतिरिक्त साधक के अन्य सभी प्रकार के अभ्यास केवल प्रयास मात्र होते हैं अर्थात् उनसे किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती ।
पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते । मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते ।। 21 ।।
भावार्थ :- जिस भी साधक ने पवन अर्थात् अपने प्राणवायु को वश में कर लिया है । वही साधक मन को भी अपने वश में कर सकता है । इस प्रकार जो मन को वश में कर लेता है । वह प्राण को भी वश में कर लेता है । विशेष :- ऊपर वर्णित श्लोक व दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी इस बात का स्प्ष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि प्राण व मन एक दूसरे के पूरक हैं । जैसे ही प्राण को वश में किया जाता है वैसे ही यह मन अपने आप वश में हो जाता है । इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता ।
हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरण: । तयोर्विनष्ट एकस्मिंस्तौ द्वावपि विनश्यत: ।। 22 ।।
भावार्थ :- चित्त के चंचल या गतिमान होने के दो प्रमुख कारण होते हैं । एक वासना और दूसरा प्राण । इन दोनों कारणों में से यदि एक कारण भी नष्ट हो जाता है तो दूसरा भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है । विशेष :- ऊपर श्लोक में चित्त की चंचलता के दो कारणों में एक कारण प्राण को बताया गया है । यहाँ पर इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राण के नष्ट हो जाने से ही चित्त की चंचलता नष्ट होगी । बल्कि यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि जो प्राण की अनियंत्रित अवस्था होती है । वह चित्त की चंचलता का कारण है न कि प्राण । यदि ऐसा होता तो प्राण के नष्ट होने पर तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा । अतः यहाँ पर प्राण का अर्थ प्राण की अनियंत्रित गति समझना चाहिए । यही सूत्रकार का कथन है ।
मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते । पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते ।। 23 ।।
भावार्थ :- जब साधक का मन सभी विषयों का त्याग कर देता है तब वह लीन अर्थात् स्थिर हो जाता है । तब मन के लीन अथवा स्थिर हो जाने से वह प्राण भी स्थिर हो जाता है ।
दुग्धाम्बुवत् सम्मिलितावुभौ तौ तुल्यक्रियौ मानसमारुतौ हि । यतो मरुत्तत्र मन: प्रवृत्तिर्यतो मनस्तत्र मरुत्प्रवृत्ति: ।। 24 ।।
भावार्थ :- जिस प्रकार दूध और पानी दोनों के मिश्रण अर्थात् दोनों को एक साथ मिला देने से वह दोनों एक ही रूप में अपना कार्य करते हैं । ठीक उसी प्रकार यह मन व प्राण भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं । जैसे ही साधक का प्राण क्रियाशील होता है वैसे ही उसका मन भी क्रियाशील हो जाता है । ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं । जिस प्रकार की दशा हमारे प्राण की होती है । ठीक वैसी ही दशा हमारे मन की हो जाती है । ठीक इसी तरह जो अवस्था हमारे मन की होती है । वही अवस्था हमारे प्राण की हो जाती है । विशेष :- इस श्लोक में दूध व पानी के मिश्रण का उदाहरण इसी लिए दिया गया है ताकि सभी विद्यार्थी आसानी से इनके ( प्राण व मन ) क्रियाकलापों को समझ सकें । जिस प्रकार दूध में पानी या पानी में दूध मिला दिया जाता है तो वह दोनों एक ही रूप में अपना काम करते हैं अलग -अलग नहीं । इसी प्रकार प्राण व मन एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं अलग- अलग नहीं ।
तत्रैकनाशादपरस्य नाश: एकप्रवृत्तेरपरप्रवृत्ति: । अध्वस्तयोश्चेन्द्रियवर्गवृत्ति: प्रध्वस्तयोर्मोक्षपदस्य सिद्धि: ।। 25 ।।
भावार्थ :- इन दोनों में से ( मन व प्राण ) यदि एक नष्ट ( उनकी गतिशीलता ) हो जाता है तो दूसरा भी स्वयं ही नष्ट हो जाता है अर्थात् दूसरे की गति का नाश भी अपने आप ही हो जाता है । ठीक इसी प्रकार एक के गतिशील होने पर दूसरा भी गतिशील हो जाता है । जब यह दोनों ( मन व प्राण ) निरन्तर गतिशील रहते हैं तो हमारी इन्द्रियाँ भी अपने – अपने विषयों में प्रवृत्त रहती हैं । लेकिन जैसे ही यह दोनों गतिविहीन हो जाते हैं अर्थात् जब इनमें स्थिरता आ जाती है । तब साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है ।
रसस्य मनसश्चैव चञ्चलत्वं स्वभावतः । रसो बद्धो मनो बद्धं किं न सिद्धयति भूतले ।। 26 ।।
भावार्थ :- मन व पारा ( पारा एक धातु है ) दोनों की प्रकृति ( स्वभाव ) चंचल होते हैं अर्थात् यह दोनों मूल रूप से चंचल होते हैं । यदि पारा धातु को बांध लिया जाए और मन को एक जगह पर स्थिर कर दिया जाए तो उस साधक के लिए ( जिसने मन को स्थिर कर लिया है ) इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा क्या है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता ? अर्थात् इस पूरी पृथ्वी पर उसके लिए सबकुछ सम्भव हो जाता है ।
मुर्च्छितो हरते व्याधीन् मृतो जीवयति स्वयम् । बद्ध: खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च पार्वति ।। 27 ।।
भावार्थ :- हे पार्वती ! पारा धातु को शोधित करने पर ( उसकी भस्म बना देने से ) और प्राण की गति को मन्द करने से यह दोनों ही रोगों को दूर करने का काम करते हैं । पारा धातु स्वयं मरके दूसरों को जीवन प्रदान करता है ( जब पारा धातु को तीव्र अग्नि में भस्म किया जाता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है अथवा उसकी स्वयं की सत्ता समाप्त हो जाती है ) । पारा बांधे जाने से और प्राण का निरोध होने पर वह ऊर्ध्वगामी होकर साधक को आकाश गमन की सिद्धि प्रदान करते हैं ।
मन: स्थैर्ये स्थिरो वायुस्ततो बिन्दु: स्थिरो भवेत् । बिन्दुस्थैर्यात् सदा सत्त्वं पिण्डस्थैर्यं प्रजायते ।। 28 ।।
भावार्थ :- मन के स्थिर हो जाने से हमारा प्राण भी स्थिर हो जाता है । जिससे वीर्य भी शरीर में स्थिर हो जाता है और वीर्य के शरीर में स्थिर होने से सदा शक्ति और स्थिरता बनी रहती है ।
इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुत: । मारुतस्य लयो नाथ: स लयो नादमाश्रित: ।। 29 ।।
भावार्थ :- हमारी सभी इन्द्रियों को नियंत्रित करने वाला अथवा उनका स्वामी मन है और उस मन को नियंत्रित करने वाला अथवा उसका स्वामी प्राण है । उस प्राण को नियंत्रित करने वाला लय होता है और वह लय नाद पर आश्रित होता है अर्थात् नाद लय का स्वामी होता है ।
सोऽयमेवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतान्तरे । मन: प्राणलये कश्चिदानन्द: सम्प्रवर्तते ।। 30 ।।
भावार्थ :- कुछ आचार्यों के मतानुसार इस लय को ही मोक्ष नाम से जाना जाता है अर्थात् लय को ही मोक्ष कहा गया है । वहीं कुछ आचार्यों के अनुसार ऐसा नहीं माना जाता । लेकिन मन और प्राण दोनों के लयबद्ध होने से साधक को एक आनन्द की अनुभूति होती है ।
प्रनष्टश्वासनि:श्वास: प्रध्वस्तविषयग्रह: । निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिनाम् ।। 31 ।।
भावार्थ :- जिस साधक के प्राणों की गति समाप्त हो गई है अर्थात् जिसने प्राणायाम द्वारा अपने श्वास- प्रश्वास को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है । जिस साधक की इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयों का पूर्ण रूप से त्याग हो चुका है अर्थात् जिस की इन्द्रियाँ पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में हो चुकी हैं । जिसकी सभी इच्छाएँ समाप्त हो चुकी हैं । जो सभी विकारों से रहित हो गया है । ऐसे योगियों को लय की प्राप्ति होती है ।
उच्छि न्नसर्व सङ्कल्पो नि:शेषाशेषचेष्टित: । स्वावगम्यो लय: कोऽपि जायते वागगोचर: ।। 32 ।।
भावार्थ :- जिस साधक के सभी संकल्प समाप्त हो गए हैं और कोई भी इच्छा शेष न बची हो अर्थात् जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं । ऐसी लय की अवस्था को स्वयं के द्वारा ही अनुभूत ( महसूस ) किया जा सकता है । वाणी द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।
यत्र दृष्टिर्लयस्त्र भूतेन्द्रियसनातनी । सा शक्तिर्जीवभूतानां द्वे अलक्ष्ये लयं गते ।। 33 ।।
भावार्थ :- जहाँ पर साधक की दृष्टि एकाग्र होती है । वहीं पर लय का स्थान होता है । वहाँ पर सभी पंच महाभूतों ( आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी ) व इन्द्रियों की परम्परागत शक्ति होती है । उस शक्ति में जीवात्मा के सभी उद्देश्य विलीन हो जाते हैं ।
लयो लय इति प्राहु: कीदृशं लयलक्षणम् । अपुनर्वासनोत्थानाल्लयो विषयविस्मृति: ।। 34 ।।
भावार्थ :- कुछ योग साधक मात्र लय- लय कहते रहते हैं । लेकिन लय होता क्या है ? यह उनको नहीं पता होता । जहाँ पर सभी वासनाएँ पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं अर्थात् जिस अवस्था में कभी भी वासना प्रबल नहीं होती । जहाँ किसी विषय की कोई भी स्मृति शेष नहीं बचती है । वह स्थिति लय की होती है ।
शाम्भवी मुद्रा वर्णन
वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । एकैक शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ।। 35 ।।
भावार्थ :- वेद, शास्त्र और पुराण आदि ग्रन्थ सामान्य व आसानी से प्राप्त होने वाले हैं । लेकिन शाम्भवी मुद्रा ही एकमात्र कुलवधू ( अच्छे परिवार की बहू ) के समान गुप्त होती है । विशेष :- इस श्लोक में सामान्य गणिका शब्द का प्रयोग किया गया है । जिसमें गणिका का सामान्य अर्थ वेश्या होता है । लेकिन इस ग्रन्थ में इसका अर्थ वेश्या नहीं है । यहाँ गणिका का अर्थ कहीं पर भी उपलब्ध होने वाला है । वेश्या को भी आसानी से कहीं पर भी उपलब्ध होने वाली माना जाता है । इसी कारण कुछ भाष्यकारों ने तो अपने अनुवाद में इसे वेश्या ही सम्बोधित किया है और कुछों ने इसका अनुवाद न करके गणिका शब्द को ही अपने अनुवाद में प्रयोग किया है । यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम वेद, शास्त्रों व पुराणों को वेश्या की संज्ञा नहीं दे सकते । क्योंकि उनके पूरे ग्रन्थ में कहीं पर भी इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है । अतः यहाँ पर गणिका शब्द का अर्थ है जो कहीं पर भी उपलब्ध हो जाए । इसका एक तर्क यह भी बनता है कि 14 वीं शताब्दी में वेद, शास्त्र व पुराणों का सभी जगह पर उपलब्ध होना एक सामान्य बात थी । आज वर्तमान समय में यह प्रमाण सही नहीं बैठता । लेकिन उस समय पर यह प्रमाण बिलकुल सही बैठता है । कुछ बातें कल प्रमाणिक थी जो आज प्रमाणिक नहीं हैं । कुछ बातें आज के समय में प्रमाणिक है लेकिन हो सकता है कि वो भविष्य में प्रमाणिक न रहें । इसलिए कुछ व्यक्ति काल भेद का अन्तर नहीं कर पाते हैं । जिसके कारण इस प्रकार की गलत धारणाएँ फैलती हैं ।
शाम्भवी विधि
अन्तर्लक्ष्यं बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता । एषा सा शाम्भवी मुद्रा वेदशास्त्रेषु गोपिता ।। 36 ।।
भावार्थ :- शाम्भवी मुद्रा में साधक के दोनों नेत्र ( आँखें ) खुली रहती हैं । लेकिन वह स्थिर होती हैं अर्थात् साधक आँखें खोलकर भी बाहर की ओर नहीं देखता । उसका लक्ष्य अन्दर की ओर ही होता है । वेद और शास्त्रों में यह विद्या गुप्त रूप से बताई गई है ।
अन्तर्लक्ष्यविलीनचित्तपवनो योगी यदा वर्तते दृष्टया निश्चलतारया बहिरध: पश्यन्नपश्यन्नपि । मुद्रेयं खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा प्रसादाद् गुरो: शून्याशून्यविलक्षणं स्फुरति तत्तत्त्वं परं शाम्भवम् ।। 37 ।।
भावार्थ :- जब योगी साधक अन्तर्लक्ष्य अर्थात् अन्दर की ओर लक्ष्य का निर्धारण करके अपने चित्त व प्राण की गति को नियंत्रित कर लेता है । तब वह बाहर व नीचे की ओर देखते हुए भी बाहर व नीचे नहीं देखता है । यह अवस्था शाम्भवी मुद्रा की होती है जो केवल गुरु की कृपा से ही मिलती है । इस अवस्था में योगी का चित्त शून्य व अशून्य दोनों ही स्थितियों से भिन्न उस परमात्मा में स्थित होता है ।
श्री शाम्भव्याश्च खेचर्या अवस्था धामभेदत: । भवेच्चित्तलयानन्द: शून्ये चित्सुखरूपिणि ।। 38 ।।
भावार्थ :- श्री शाम्भवी मुद्रा व खेचरी मुद्रा के स्थान व अवस्था दोनों में ही अन्तर होता है । लेकिन शून्य अवस्था में चित्त का लय होने पर दोनों में ही चित्त में विशेष प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है ।
तारे ज्योतिषी संयोज्य किञ्चिदुन्नमयेद् भ्रुवौ । पूर्वयोगं मनो युञ्जन्नुन्मनीकारक: क्षणात् ।। 39 ।।।
भावार्थ :- भ्रुमध्य में स्थित आज्ञाचक्र में मन को स्थिर करके अपनी दोनों भौहों ( दोनों आँखों के बीच का स्थान ) को थोड़ा ऊपर की ओर उठाएं । इसके बाद साधक पहले से बताई गई विधि के अनुसार अपने मन व प्राण को स्थिर करके शीघ्रता से समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है ।
केचिदागमजालेन केचिन्निगमसङ्कुलै: । केचित्तर्केण मुह्यन्ति नैव जानन्ति तारकम् ।। 40 ।।
भावार्थ :- कुछ योगी साधक तो आगम ( शिव द्वारा उपदेशित ग्रन्थ ) के जाल में व कुछ साधक वैदिक वाङ्गमय के आपसी चक्रों में पड़ जाते हैं । वहीं कुछ आपसी तर्क- वितर्कों में ही उलझकर मार्ग से भटक जाते हैं । वे उस मुक्ति प्रदान करने वाली उन्मनीकला ( समाधि ) को जान ही नहीं पाते हैं ।
अर्धोन्मीलितलोचन: स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षण: चन्द्रर्कावपि लीनतामुपनयन्निस्पन्दभावेन य: । ज्योतीरूपमशेषबीजमखिलं देदीप्यमानं परम् तत्त्वं तत्पदमेति वस्तु परमं वाच्यं किमत्राधिकम् ।। 41 ।।
भावार्थ :- जो योग साधक अपने दोनों नेत्रों को आधा खोलकर, मन को एक जगह पर स्थिर करके, अपनी दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर केन्द्रित करके, पूर्ण रूप से स्थिर होकर व जिसने इडा व पिङ्गला नाड़ियों में चलते हुए प्राण को नियंत्रित कर लिया हो । वह साधक ज्योति स्वरूप से भी ज्यादा दीप्तिमान जिसे परमात्मा कहा जाता है । उसे देखता हुआ उसी परमपद को प्राप्त कर लेता है ।
दिवा न पूजयेल्लिङ्गं रात्रौ चैव न पूजयेत् । सर्वदा पूजयेल्लिङ्गं दिवारात्रिनिरोधत: ।।42 ।।
भावार्थ :- साधक को लिङ्ग ( परमात्मा ) की उपासना या आराधना न ही तो दिन में ( पिङ्गला नाड़ी में ) करना चाहिए और न ही रात्रि में ( इडा नाड़ी में ) बल्कि उसे दिन व रात ( इडा व पिङ्गला ) दोनों का ही निरोध होने पर ( सुषुम्ना नाड़ी के चलने पर ही ) लिङ्ग ( परमात्मा ) की उपासना अथवा आराधना करनी चाहिए । विशेष :- इस श्लोक में पिङ्गला व इडा को ही क्रमशः दिन व रात कहकर सम्बोधित किया गया है । पिङ्गला का अर्थ है सूर्य नाड़ी चूँकि सूर्य दिन में ही निकलता है और सूर्य ही पिङ्गला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है । इसी प्रकार इडा का अर्थ है चन्द्र नाड़ी चूँकि चन्द्रमा रात में ही निकलता है और चन्द्रमा ही इडा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है । इसलिए यहाँ पर पिङ्गला व इडा को क्रमशः दिन व रात कहा गया है । तभी कहा गया है कि दोनों का निरोध होने पर ही अर्थात् इडा व पिङ्गला का निरोध होने पर ही लिङ्ग की उपासना करनी चाहिए । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी के क्रियाशील होने पर ही उपासना करनी चाहिए । उसके अतिरिक्त उपासना करने से वह सिद्ध नहीं होती है ।
खेचरी मुद्रा वर्णन
सव्यदक्षिणनाडिस्थो मध्ये चरति मारुत: । तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने न संशय: ।। 43 ।।
भावार्थ :- चन्द्र ( बायीं नासिका ) व सूर्य ( दायीं नासिका ) में चलने वाली प्राणवायु जब बीच में अर्थात् सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगती है । तब वह खेचरी मुद्रा की अवस्था होती है । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।
इडापिङ्गलयोर्मध्ये शून्यं चैवानिलं ग्रसेत् । तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं पुनः पुनः ।। 44 ।।
भावार्थ :- इडा व पिङ्गला नाड़ियों के बीच में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणवायु का ग्रहण होता है तब वहाँ पर खेचरी मुद्रा स्थित होती है । यह बात पूर्ण रूप से सत्य है ।
सूर्याचन्द्रमसोर्मध्ये निरालम्बान्तरे पुनः । संस्थिता व्योमचक्रे सा या मुद्रा नाम खेचरी ।। 45 ।।
भावार्थ :- एक बार फिर जो इडा व पिङ्गला नाड़ियों के बीच में अर्थात् सुषुम्ना नाड़ी में बिना किसी की सहायता के जो व्योमचक्र ( आकाश में ) स्थित है । वह खेचरी मुद्रा है ।
सोमाद्यत्रोदिता धारा साक्षात् सा शिववल्लभा । पूरयेदतुलां दिव्यां सुषुम्नां पश्चिमे मुखे ।। 46 ।।
भावार्थ :- सोममण्डल अर्थात् चन्द्र नाड़ी से बहने वाली धारा साक्षात भगवान शिव की प्रिय है । उस सोमधारा को पीछे के मार्ग से अर्थात् मेरुदण्ड के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी में भर देना चाहिए ।
पुरस्ताच्चैव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत् । अभ्यस्ता खेचरी मुद्राप्युन्मनी सम्प्रजायते ।। 47 ।।
भावार्थ :- इस प्रकार उस सोमधारा को सुषुम्ना नाड़ी में भर देने पर निश्चित रूप से खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है । इस प्रकार इस खेचरी मुद्रा के अभ्यास से उन्मनी अर्थात् समाधि की सिद्धि होती है ।
भ्रुवोर्मध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते । ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्यं तत्र कालो न विद्यते ।। 48 ।।
भावार्थ :- दोनों भौहों के बीच में जो स्थान होता है उसे भगवान शिव का स्थान कहा गया है । जिसे तन्त्र की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं । साधक को अपना मन वहाँ पर विलीन अर्थात् स्थिर कर देना चाहिए । वहाँ पर काल का बोध ( मृत्यु ) अथवा ज्ञान नहीं होता । जिससे साधक मृत्यु को जीत कर समाधि की प्राप्ति कर लेता है ।
अभ्यसेत् खेचरीं तावद्यात् स्याद्योगनिद्रित: । सम्प्राप्तयोगनिद्रस्य कालो नास्ति कदाचन ।। 49 ।।
भावार्थ :- साधक को इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि वह योगनिद्रा ( समाधि ) को प्राप्त नहीं कर लेता । जैसे ही साधक को योगनिद्रा की प्राप्ति ( समाधि ) हो जाती है । वैसे ही उसे काल ( मृत्यु ) का कोई डर नहीं रहता ।
निरालम्बं मन: कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् । स बाह्याभ्यन्तरे व्योम्नि घटवत्तिष्ठति ध्रुवम् ।। 50 ।।
भावार्थ :- जब साधक अपने मन को सभी प्रकार के विचारों से मुक्त कर देता है और साथ ही मन के सभी प्रकार के संकल्प- विकल्पों को रोक देता है । तब साधक बाहर और भीतर से ठीक उसी प्रकार से स्थिर हो जाता है । जैसे कि घड़ा एक जगह पर स्थिर रहता है ।
बाह्यावायुर्यथा लीनस्तथा मध्यो न संशय: । स्वस्थाने स्थिरतामेति पवनो मनसा सह ।। 51 ।। भावार्थ :- जिस प्रकार बाहर से लिया जाने वाला प्राणवायु स्थिर हो जाता है । उसी प्रकार मध्ये अर्थात् शरीर के अन्दर स्थित प्राणवायु भी स्थिर हो जाता है । तब अपने स्थान पर स्थित प्राणवायु मन के साथ मिलकर स्थिर हो जाती है । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।
एवमभ्यसमानस्य वायुमार्गे दिवानिशम् । अभ्यासाज्जीर्यते वायुर्मनस्तत्रैव लीयते ।। 52 ।। भावार्थ :- ऊपर वर्णित विधि के अनुसार प्राणवायु का दिन – रात अभ्यास करने से साधक प्राणवायु को जीत लेता है । जिससे प्राण गतिविहीन अथवा स्थिर हो जाता है । इस अवस्था में प्राण के साथ मन भी लीन ( स्थिर ) हो जाता है ।
अमृतै: प्लावयेद्देहमापादतलमस्तकम् । सिद्धयत्येव महाकायो महाबलपराक्रम् ।। 53 ।। भावार्थ :- ऊपर वर्णित साधना साधक को पैर से लेकर सिर तक सोमरस रूपी अमृत से परिपूर्ण ( भर ) कर देती है । जिससे साधक का शरीर विशाल ( बड़ा ) व अत्यन्त बल व पराक्रम से युक्त हो जाता है ।
शक्तिमध्ये मन: कृत्वा शक्तिं मानसमध्यगाम् । मनसा मन आलोक्य धारयेत् परमं पदम् ।। 54 ।। भावार्थ :- पहले साधक अपने मन को कुण्डलिनी शक्ति में स्थिर करे ( लगाए ) और फिर कुण्डलिनी शक्ति को मन में स्थिर करे । इस प्रकार योगी अपने मन को अपने ही मन में स्थिर करता हुआ उस परमपद अर्थात् सर्वोच्य पद ( समाधि ) को प्राप्त कर लेता है ।
खमध्ये कुरुचात्मानमात्ममध्ये च खं कुरु । सर्वं च खमयं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।। 55 ।। भावार्थ :- मैं आकाश में और आकाश मुझमें स्थित है । इस प्रकार के भाव का ही विचार साधक को करना चाहिए । साथ ही सभी को ब्रह्म का अंश मानकर केवल उसी का चिन्तन अथवा उपासना करनी चाहिए । अन्य किसी की नहीं ।
अन्त: शून्यो: बहि: शून्य: कुम्भ इवाम्बरे । अतः पूर्णो बहि: पूर्ण: पूर्ण: कुम्भ इवार्णवे ।। 56 ।। बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथैवान्तरचिन्तनम् । सर्वचिन्तां परित्यज्य न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।। 57 ।। भावार्थ :- जिस प्रकार खाली घड़े के बाहर और अन्दर का हिस्सा खाली रहता है अर्थात् वह शून्य स्थान कहलाता है । जिसे हम आकाश की संज्ञा देते हैं । ठीक इसी प्रकार पानी में डूबा हुआ घड़ा जिस प्रकार अन्दर व बाहर दोनों प्रकार से ही पानी से युक्त होता है अर्थात् उस घड़े के अन्दर भी जल होता है और उसके बाहर भी जल होता है । अतः जिस तरह घड़ा अन्दर व बाहर दोनों ही प्रकार से पूर्ण होता है ठीक उसी प्रकार योगी को भी साधना काल में सभी बाह्य ( बाहरी ) व आन्तरिक ( अन्दर ) विचारों का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार योगी सभी बाहरी व भीतरी विचारों से पूरी तरह से शून्य होकर साधना करे ।
सङ्कल्पमात्रकलनैव जगत् समग्रम् सङ्कल्पमात्रकलनैव मनोविलास: । सङ्कल्पमात्रमतिमुत्सृज निर्विकल्पमाश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि राम शान्तिम् ।। 58 ।। भावार्थ :- हे राम! यह सम्पूर्ण जगत ( संसार ) हमारे मन की कल्पना मात्र ही है और इस जगत ( संसार ) की जितनी भी काल्पनिक रचनाएं हैं वह भी केवल हमारे मन की ही उपज ( देन ) है । अतः साधक को अपने मन द्वारा उपजी इस कल्पना के आश्रय को छोड़कर शान्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ।
कर्पूरमनले यद्वत् सैन्धवं सलिले यथा । तथा सन्धीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते ।। 59 ।। भावार्थ :- जिस तरह अग्नि में डालने से कपूर अपना स्वरूप खोकर अग्नि के अन्दर विलीन ( लीन ) हो जाता है । तथा पानी में मिलाने पर जिस प्रकार नमक अपने स्वरूप को खोकर पानी में विलीन हो जाता है । ठीक इसी प्रकार मन को ब्रह्म तत्त्व में लगाने से वह मन भी अपना स्वरूप खोकर ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है ।
ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्य: पन्था द्वितीयक: ।। 60 ।। भावार्थ :- जो भी पदार्थ जाने जाते हैं वह सभी ज्ञान के विषय हैं और मन भी ज्ञान का ही विषय है । इस तरह ज्ञान व ज्ञान को जानने वाले अर्थात् मन दोनों को ही विलीन करने से ही उस लय का मार्ग प्रशस्त ( मिलता ) होता है । इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है ।
मनोदृश्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् सचराचरम् । मनसो ह्युन्मनीभावाद् द्वैतं नैवोपलभ्यते ।। 61 ।। भावार्थ :- यह सभी चर व अचर दिखाई देने वाला सम्पूर्ण जगत हमारे मन का ही विषय है अर्थात् यह सब मन के द्वारा ही सम्भव हो पाता है । जैसे ही हमारा मन उन्मनी भाव ( समाधि ) को प्राप्त कर लेता है । वैसे ही द्वैत भाव ( दो प्रकार का विचार ) भी समाप्त हो जाता है ।
ज्ञेयवस्तुपरित्यागाद्विलयं याति मानसम् । मनसो विलये जाते कैवलयमवशिष्यते ।। 62 ।। भावार्थ :- जो भी ज्ञेय अर्थात् ज्ञान या जानकारी करवाने वाले पदार्थों का त्याग करने से मन भी ब्रह्म में लीन हो जाता है । इस तरह मन के ब्रह्म में लीन होने से साधक को कैवल्य ( समाधि ) की प्राप्ति हो जाती है ।
एवं नानाविधोपाया: सम्यक् स्वानुभवान्विता: । समाधि मार्गा: कथिता: पूर्वाचार्यैर्महात्मभि: ।। 63 ।। भावार्थ :- इस प्रकार पहले उत्पन्न हुये महान योग आचार्यों ने अपनी योग साधना के समय के अनुभवों से समाधि की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की योग विधियों का उपदेश दिया है ।
सुषुम्नायै कुण्डलिन्यै सुधायै चन्द्रजन्मने । मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने ।। 64 ।। भावार्थ :- हे सुषुम्ना, कुण्डलिनी, चन्द्रमा से उत्पन्न अमृत, मनोन्मनी अवस्था ( समाधि ) व चित्त स्वरूप महाशक्ति आप सबको प्रणाम है । विशेष :- ऊपर वर्णित सभी शब्द समाधि को ही परिभाषित करते हैं । अतः सूत्रकार इनको विशेष महत्त्व देते हुए इन सबको प्रणाम करता है ।
नादानुसन्धान वर्णन
अशक्यतत्त्वबोधानां मूढानामपि सम्मतम् । प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते ।। 65 ।। भावार्थ :- जिन निम्न कोटि के योग साधकों को उस परम तत्त्व का ज्ञान नहीं हो पाता है । उन सभी के लिए गुरु गोरक्षनाथ द्वारा स्वीकृत ( मानी गई ) नादयोग उपासना की विधि का वर्णन किया गया है ।
श्री आदिनाथेन सपादकोटिलयप्रकारा: कथिता जयन्ति । नादानुसन्धानकमेकमेव मन्यामहे मुख्यतमं लयानाम् ।। 66 ।। भावार्थ :- श्री आदिनाथ शिव ( भगवान शिव ) के द्वारा नादयोग साधना के सवा करोड़ प्रकार बताए हैं अर्थात् भगवान शिव ने नादयोग साधना की सवा करोड़ विधियों का वर्णन किया है । उनमें से मैं नादयोग को सबसे महत्त्वपूर्ण मानता हूँ ।
मुक्तासने स्थितो योगी मुद्रां सन्धाय शाम्भवीम् । शृणुयाद्देक्षिणे कर्णे नादमन्तस्थमेकधी: ।। 67 ।। भावार्थ :- इसके लिए सबसे पहले साधक मुक्तासन की स्थिति में बैठकर शाम्भवी मुद्रा को लगाए । इसके बाद पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर अपने दायें कान से शरीर के अन्दर से आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करे ।
श्रवणपुटनयनयुगल घ्राणमुखानां निरोधनं कार्यम् । शुद्धसुषुम्नासरणौ स्फुटममल: श्रूयते नाद: ।। 68 ।। भावार्थ :- जब साधक अपने दोनों कान, दोनों आँख, नासिका के दोनों छिद्रों और मुहँ को बन्द कर लेता है । तब उसे पूरी तरह से शुद्ध सुषुम्ना मार्ग से पूरी तरह से स्पष्ट व पवित्र नाद सुनाई पड़ता है ।
नादयोग की चार अवस्थाएँ
आरम्भश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च । निष्पत्ति: सर्वयोगेषु स्यादवस्थाचतुष्टयम् ।। 69 ।। भावार्थ :- सभी प्रकार की योग साधना पद्धतियों में मुख्य रूप से चार प्रकार की अवस्थाएँ पाई जाती हैं । जिन्हें क्रमशः आरम्भ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था व निष्पत्ति अवस्था कहा जाता है । विशेष :- इस श्लोक में नादयोग की सभी अवस्थाओं को क्रमानुसार दर्शाया गया है । परीक्षा की दृष्टि से भी यह श्लोक अति महत्त्वपूर्ण है । बहुत बार नाद की पहली से लेकर अन्तिम अवस्था तक इनके सही क्रम को पूछा जाता है । अतः सभी विद्यार्थी इनके इस क्रम को याद करलें ।
आरम्भ अवस्था के लक्षण
ब्रह्मग्रन्थेर्भवेद् भेदादानन्द: शून्यसम्भव: । विचित्र: क्वणको देहेऽनाहत: श्रूयते ध्वनि: ।। 70 ।। दिव्यदेहसश्च तेजस्वी दिव्यगन्धस्त्वरोगवान् । सम्पूर्णहृदय: शून्य आरम्भे योगवान् भवेत् ।। 71 ।। भावार्थ :- नादयोग की पहली अवस्था में साधक की ब्रह्मग्रन्थि का भेदन हो जाता है । जिससे साधक विचार शून्य अर्थात् विचारों से रहित हो जाता है । विचार शून्यता के परिणाम स्वरूप उसे दिव्य आनन्द की अनुभूति ( अहसास ) होती है । शरीर में असाधारण प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं । साधक का शरीर दिव्य गन्ध व दिव्य तेज से युक्त हो जाता है । वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है साथ ही उसका चित्त प्रसन्न होकर शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है ।
घटावस्था के लक्षण
द्वितीयायां घटीकृत्य वायुर्भवति मध्यग: । दृढासनो भवेद्योगी ज्ञानी देवसमस्ततथा ।। 72 ।। विष्णुग्रन्थेस्ततो भेदात् परमानन्दसूचक: । अतिशून्ये विमर्दश्च भेरीशब्दस्तदा भवेत् ।। 73 ।। भावार्थ :- दूसरी अवस्था अर्थात् नाद की घटवस्था में प्राणवायु शरीर को घड़ा बनाकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है । जिससे साधक का आसन मजबूत हो जाता है और योगी के अन्दर देवताओं के समान ज्ञान हो जाता है । जिसके बाद उस साधक की विष्णु ग्रन्थि का भेदन ( खुल जाना ) हो जाता है । तब साधक शून्यभाव होकर परम आनन्द को देने वाले विमर्द और भेरी ( वाद्ययंत्र ) नामक शब्दों को सुनता है
परिचय अवस्था के लक्षण
तृतीयायां तु विज्ञेयो विहायो मर्दलध्वनि: । महाशून्यं तदा याति सर्वसिद्धि समाश्रयम् ।। 74 ।। चित्तानन्दं तदा जित्वा सहजानन्दसम्भव: । दोषदुःखजराव्याधिक्षुधानिद्राविवर्जित: ।। 75 ।। भावार्थ :- नादयोग की इस तीसरी अवस्था में साधक को हृदय आकाश में मर्दल नामक वाद्ययंत्र की ध्वनि सुनाई देती है । प्राण सभी सिद्धियों को प्रदान करवाने वाले उस आकाश तत्त्व में पहुँच कर वहाँ स्थित विशुद्धि चक्र का भेदन करता है । जिसके परिणाम स्वरूप साधक को सहजानन्द की प्राप्ति होती है । इसके अलावा योगी सभी दोषों ( वात, पित्त, कफ ), सभी प्रकार के दुःखों, बुढ़ापा, सभी रोगों, भूख व निद्रा से मुक्त हो जाता है ।
निष्पत्ति अवस्था के लक्षण
रुद्रग्रन्थिं यदा भित्वा शर्वपीठगतोऽनिल: । निष्पत्तौ वैणव: शब्द: क्वणद्वीणाक्वणो भवेत् ।। 76 ।। एकीभूतं तदा चित्तं राजयोगाभिधानकम् । सृष्टिसंहारकर्तासौ योगीश्वरसमो भवेत् ।। 77 ।। भावार्थ :- नादयोग की चौथी अवस्था अर्थात् निष्पत्ति में साधक का प्राण रुद्रग्रन्थि का भेदन करके आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है । जिसके परिणाम स्वरूप साधक को वीणा नामक अत्यन्त मनमोहक वाद्ययन्त्र की ध्वनि सुनाई देती है । साथ ही चित्त एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है । जिसे राजयोग नामक समाधि कहा जाता है । इस अवस्था में साधक में ईश्वर के समान सृष्टि को बनाने व नष्ट करने का सामर्थ्य आ जाता है ।
अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिरत्रै वाखण्डितं सुखम् । लयोद् भवमिदं सौख्यं राजयोगादवाप्यते ।। 78 ।। भावार्थ :- साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो या न हो लेकिन राजयोग समाधि के परिणाम स्वरूप उसके चित्त में लय के उत्पन्न होने से उसे बिना खण्डित हुए ( निरन्तर मिलने वाले ) आनन्द की प्राप्ति होती है ।
राजयोग का महत्व
राजयोगमजानन्त: केवलं हठकर्मिण: । एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफलवर्जितान् ।। 79 ।। भावार्थ :- जो योगाभ्यासी राजयोग को नहीं जानते और केवल हठयोग साधना का ही अभ्यास करते रहते हैं । मैं उन सभी साधकों के परिश्रम को निष्फल या निरर्थक ( जिससे किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती ) मानता हूँ ।
उन्मन्यवाप्तये शीघ्रं भ्रुध्यानं मम सम्मतम् । राजयोगपदं प्राप्तुं सुखो पायोऽल्पचेतसाम् । सद्य: प्रत्ययसन्धायी जायते नादजो लय: ।। 80 ।। भावार्थ :- जो साधक साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपनी दोनों भौहों के बीच में ध्यान लगाना चाहिए । इससे साधक को शीघ्र उन्मनी भाव ( समाधि ) की प्राप्ति होती है । ऐसा मेरा मानना है । इसके अलावा जिन योग साधकों को योग विषय में कम ज्ञान है या जो योग साधना को ज्यादा नहीं जानते। उनके लिए समाधि प्राप्ति हेतु नादयोग की साधना शीघ्र ही सुख व विश्वास उत्पन्न करवाने वाली सिद्ध होती है ।
नादानुसन्धानसमाधिभाजाम् योगीश्वराणां हृदि वर्धमानम् । आनन्दमेकं वचसामगम्यम् जानाति तं श्रीगुरुनाथ एक: ।। 81 ।। भावार्थ :- जिन साधकों ने नादानुसन्धान के द्वारा समाधि की प्राप्ति हो जाती है । उन सभी श्रेष्ठ योगियों के हृदय में एक विशेष प्रकार के अद्भुत व अवर्णनीय ( जिसका वर्णन वाणी के द्वारा न किया जा सके ) आनन्द की प्राप्ति होती है । इस आनन्द को तो वह साधक ही जानता है जिसने समाधि के द्वारा उसे प्राप्त किया है । उसके अतिरिक्त केवल श्रीगुरुनाथ अर्थात् गुरु गोरक्षनाथ ही जानते हैं ।
कर्णौ पिधाय हस्ताभ्यां यं शृणोति ध्वनिं मुनि: । तत्र चित्तं स्थिरी कुर्याद्यावत् स्थिरपदं व्रजेत् ।। 82 ।। भावार्थ :- जो योग साधक अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को बन्द करने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनकर उसी पर अपने चित्त को लगा लेता है । वही साधक स्थिरपद ( मोक्ष ) को प्राप्त करता है ।
अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वनिम् । पक्षाद्विक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत् ।। 83 ।। भावार्थ :- ऊपर वर्णित नादयोग विधि का अभ्यास करने पर साधक की सभी बाहरी ध्वनियाँ रुक जाती हैं । जिसके फलस्वरूप साधक मात्र पन्द्रह ( 15 ) दिनों में ही सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करके सुखी हो जाता है ।
श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान् । ततोऽभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मक: ।। 84 ।। भावार्थ :- साधना के प्रारम्भ में साधक को समुद्र की गर्जना, मेघ की गर्जना ( बादलों की गड़गड़ाहट ), भेरी नामक वाद्ययंत्र व झर्झर ( झरने ) के समान ध्वनियाँ सुनाई देती हैं । साधना काल के बीच में साधक को मर्दल ( ढोल ), शंख, घण्टा व घड़ियाल ( मगरमच्छ ) आदि के समान ध्वनियाँ सुनाई देती हैं ।
आदौ जलधिजीमूतभेरीझर्झरसम्भवा: । मध्ये मर्दलशङ्खोत्था घण्टा काहल जास्तथा ।। 85 ।। भावार्थ :- साधना के प्रारम्भ में साधक को समुद्र की गर्जना, मेघ की गर्जना ( बादलों की गड़गड़ाहट ), भेरी नामक वाद्ययंत्र व झर्झर ( झरने ) के समान ध्वनियाँ सुनाई देती हैं । साधना काल के बीच में साधक को मर्दल ( ढोल ), शंख, घण्टा व घड़ियाल ( मगरमच्छ ) आदि के समान ध्वनियाँ सुनाई देती हैं ।
अन्ते तु किङ्किणीवंशवीणाभ्रमरनि:स्वना: । इति नानाविधा नादा: श्रूयन्ते देहमध्यगा: ।। 86 ।। भावार्थ :- नादयोग साधना के अन्त में साधक को घुंघुरू, वंशी ( बाँसुरी ), वीणा ( अत्यन्य मनमोहक वाद्ययंत्र ) और भँवरे के समान ध्वनियाँ व सुषुम्ना में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के स्वर सुनाई पड़ते हैं ।
महति श्रूयमाणेऽपि मेघभेर्यादिके ध्वनौ । तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नादमेव परा मृशेत् ।। 87 ।। भावार्थ :- साधक को बादल के गरजने व भेरी जैसे तीव्र ध्वनि वाले नाद सुनाई देने पर भी उसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ध्वनियों को ही सुनने की कोशिश करनी चाहिए ।
घनमृत्युज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्ममृत्युज्य वा घने । रममाणमपि क्षिप्तं मनो नान्यत्र चलायेत् ।। 88 ।। भावार्थ :- जब नाद को सुनते हुए हमारा मन तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म ध्वनि की ओर या सूक्ष्म ध्वनि से तीव्र ध्वनि की ओर घूमता रहता है तो भी साधक को अपने चंचल मन को इन ध्वनियों से अलग अन्य कहीं पर नहीं लेकर जाना चाहिए । तात्पर्य यह है कि साधक अपने मन को इन्ही ध्वनियों के मध्य रखे । इनके अतिरिक्त कहीं अन्य स्थान पर मन को नहीं लेकर जाना चाहिए ।
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मन: । तत्रैव सुस्थिरीभूय तेन सार्धं विलीयते ।। 89 ।। मकरन्दं पिबन् भृङ्गो गन्धं नापेक्षते यथा । नादासक्तं तथा चित्तं विषयान्न हि काङ्क्षते ।। 90 ।। भावार्थ :- जब साधक का मन पहली बार किसी प्रकार के नाद ( ध्वनि ) को सुनता है तो उसका मन उसी ध्वनि के साथ लग जाता है और उसी नाद के साथ मन का एकीकरण ( मिलन ) हो जाता है अर्थात् जहाँ पर जिस भी नाद में एक बार मन लगता है तो वह वहीं पर उसके साथ लीन हो जाता है । जिस प्रकार फूलों के रस को पीने वाला भँवरा ( एक प्रकार का कीट ) उस रस की गन्ध की परवाह नहीं करता । ठीक उसी प्रकार जब साधक का मन नाद में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो उसका मन किसी भी बाहरी विषय की कोई लालसा नहीं रखता है ।
मनोमत्तगजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारिण: । नियन्त्रणे समर्थोऽयं निनादनिशिताङ्कुश: ।। 91 ।। भावार्थ :- विषय रूपी उद्यान ( बाग ) में विचरण ( घूमने ) करने वाले मन रूपी मतवाले ( अपनी मस्ती में घूमने वाला ) हाथी को वश में करने के लिए नाद रूपी तीव्र नोक वाला हथियार ही समर्थ ( उपयोगी ) होता है । विशेष :- हाथी को वश में करने के लिए उसका महावत ( हाथी की देखभाल व उसे चलाने वाला ) तेज नोक वाले हथियार का प्रयोग करता है । यहाँ पर नाद को तीव्र नोक वाले हथियार के रूप में सम्बोधित किया गया है ।
बद्धं तु नादबन्धेन मन: संत्यक्तचापलम् । प्रयाति सुतरां स्थर्यं छिन्नपक्ष: खगो यथा ।। 92 ।। भावार्थ :- नादयोग के प्रभाव से हमारा मन अपनी चंचलता को छोड़ कर इस प्रकार स्थिर हो जाता है । जिस प्रकार एक पंख कटा हुआ पक्षी उड़ने में असमर्थ होने के कारण एक जगह स्थिर हो जाता है ।
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ।। 93 ।। भावार्थ :- जो योग साधक योग साधना में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं । उन्हें अपनी सभी प्रकार की चिन्ताओं का त्याग करके मन को एकाग्र करते हुए केवल नादानुसन्धान का ही अभ्यास करना चाहिए ।
नादोन्तरङ्गसारङ्गबन्धने वागुरायते । अन्तरङ्कुरङ्गस्य वधे व्याधायतेऽपि च ।। 94 ।। भावार्थ :- मृग ( हिरण ) रूपी चंचल मन की चंचलता को बान्धने के लिए नादानुसन्धान का अभ्यास रस्सी की तरह काम करता है । जिस प्रकार चंचल हिरण को रस्सी या जाल से बान्ध कर एक जगह स्थिर किया जा सकता है । ठीक उसी प्रकार चंचल मन को स्थिर करने के लिए नादानुसंधान का अभ्यास करना चाहिए । साथ ही जिस प्रकार व्याध ( शेर ) हिरण को मार डालता है । ठीक उसी प्रकार नादानुसंधान रूपी शेर चंचल हिरण रूपी मन को मार देता है अर्थात् वह मन को अपने अन्दर लीन कर लेता है ।
अन्तरङ्गस्य यमिनो वाजिन: परिघायते । नादोपास्तिरतो नित्यमवधार्या हि योगिना ।। 95 ।। भावार्थ :- यह नादानुसंधान की साधना मन रूपी घोड़े को रोकने के लिए चारदीवारी का कार्य करती है । जिस प्रकार घोड़ो को रोकने के लिए एक उनको एक प्रकार की ऊंची चारदीवारी की आवश्यकता होती है । इसलिए योगी को मन की चंचलता को रोकने के लिए नित्य प्रति नादानुसंधान की साधना करनी चाहिए ।
बद्धं विमुक्तचाञ्चल्यं नादगन्धकजारणात् । मन: पारदमाप्नोति निरालम्बाख्यखेऽटनम् ।। 96 ।। भावार्थ :- स्थिर अथवा बाँधा हुआ मन रूपी पारे को गन्धक रूपी नादानुसंधान से भस्म करने के बाद वह प्रभावहीन ( क्रियाहीन ) हो जाता है अथवा स्थिर हो जाता है । ठीक उसी प्रकार नादानुसंधान द्वारा एक जगह स्थिर किया हुआ मन भी बिना किसी आश्रय के आकाश में स्थित अथवा लीन हो जाता है ।
नादश्रवणत: क्षिप्रमन्तरङ्गभुजङ्गम: । विस्मृत्य सर्वमेकाग्र: कुत्रचिन्न हि धावति ।। 97 ।। भावार्थ :- जिस प्रकार सांप बीन ( एक प्रकार का वाद्ययंत्र ) को सुनकर अति शीघ्रता से एकाग्र होकर उस ध्वनि ध्यान पूर्वक सुनता है । ठीक उसी प्रकार नाद की ध्वनि को सुनने के बाद सर्प ( सांप ) रूपी मन भी सबकुछ छोड़कर अति शीघ्रता से एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है । अन्य किसी विषय के बारे में बिलकुल भी नहीं सोचता ।
काष्ठे प्रवर्तितो वह्नि: काष्ठेन सह शाम्यति । नादे प्रवर्तितं चित्तं नादेन सह लीयते ।। 98 ।। भावार्थ :- जिस तरह लकड़ी में लगी हुई आग उस लकड़ी के समाप्त होने पर स्वयं ही समाप्त हो जाती है । ठीक उसी तरह नाद में लगा हुआ मन भी उस नाद में ही विलीन अथवा लीन हो जाता है ।
घण्टादिनादसक्तस्तब्धान्त: करणहरिणस्य । प्रहरणमपि सुकरं शरसन्धानप्रवीणश्चेत् ।। 99 ।। भावार्थ :- जिस प्रकार घण्टा आदि वाद्ययंत्रों की ध्वनि को सुनकर हिरण उसी में अपने को एकाग्र करके एक जगह पर स्थिर हो जाता है । उस समय धनुर्धर रूपी साधक अपनी कुशल धनुर्विद्या रूपी नाद द्वारा उस हिरण रूपी मन का आसानी से शिकार कर सकता है अर्थात् वह चंचल मन को नाद रूपी बाण द्वारा भेद सकता है । जिससे मन आसानी से नाद के साथ लीन हो जाता है ।
अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर्य उपलभ्यते । ध्वनेरन्तर्गतं ज्ञेयं ज्ञेयस्यान्तर्गतं मन: । मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णो: परमं पदम् ।। 100 ।। भावार्थ :- अनाहत नाद से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी के अन्दर जानने योग्य ब्रह्मा का निवास स्थान है और उस अनाहत नाद में ही हमारा मन पूरी तरह से लीन हो जाता है । इस स्थिति को विष्णु का परमपद अर्थात् सर्वोच्य स्थान कहा जाता है ।
तावदाकाशसङ्कल्पो यावच्छब्द: प्रवर्तते । नि:शब्दं तत् परं ब्रह्म परमात्मेति गीयते ।। 101 ।। भावार्थ :- जहाँ तक आकाश की सीमा होती है वहीं तक नाद अर्थात् शब्द की सीमा होती है । इसका तात्पर्य यह है कि शब्द की उत्पत्ति आकाश नामक महाभूत से होती है । इसलिए जहाँ तक आकाश स्थित है वहीं तक शब्द अर्थात् नाद को सुना जा सकता है । जैसे ही शब्द को सुनने की सीमा समाप्त हो जाती है अर्थात् शून्य अवस्था आ जाती है । वैसे ही वह परब्रह्म अर्थात् परमात्मा की अवस्था आ जाती है । शब्द शून्यता को ही परमात्मा कहा जाता है ।
यत् किञ्चिन्नादरूपेण श्रूयते शक्तिरेव सा । यस्तत्त्वान्तो निराकार: स एव परमेश्वर: ।। 102 ।। भावार्थ :- जो भी नाद के रूप में हम ध्वनियाँ सुनाई देती हैं । वह शक्ति का ही रूप होता है और जहाँ पर इन तत्त्वों का अन्त हो जाता है अर्थात् जहाँ पर ये तत्त्व विलीन हो जाते हैं । वही परम तत्त्व अर्थात् परमात्मा है ।
सर्वे हठलयोपाया: राजयोगस्य सिद्धये । राजयोगसमारूढ: पुरुष: कालवञ्चक: ।। 103 ।। भावार्थ :- हठयोग व लययोग की सभी साधना पद्धतियों का एकमात्र लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति करना होता है । जो भी योगी हठयोग व लययोग साधना द्वारा राजयोग रूपी समाधि की प्राप्ति कर लेता है । वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है ।
तत्त्वं बीजं हठ: क्षेत्रमौदासीन्यं जलं त्रिभि: । उन्मनी कल्पलतिका सद्य: एव प्रवर्तते ।। 104 ।। भावार्थ :- तत्त्व अर्थात् परमतत्त्व बीज के रूप में होता है और हठयोग साधना उस बीज के लिए भूमि ( खेत ) का काम करता है । साथ ही वैराग्य जल स्वरूप ( जल का प्रतिनिधि ) होता है । इन तीनों के एकसाथ मिलने से समाधि रूपी कल्पलता ( पौधा ) अति शीघ्र बढ़ने लगता है । तात्पर्य यह है कि हठयोग उपजाऊ भूमि है, वैराग्य उसको जल की आपूर्ति करता है । जिससे समाधि रूपी बेल या पौधा शीघ्रता से बढ़ने लगता है जिससे साधक को उस परम तत्त्व की प्राप्ति होती है ।
सदा नादानुसन्धानात् क्षीयन्ते पापसञ्चया: । निरञ्जने विलीयेते निश्चितं चित्त मारुतौ ।। 105 ।। भावार्थ भावार्थ :- निरन्तरता के साथ नादानुसन्धान का अभ्यास करने वाले साधक के पाप अर्थात् दुःख के सारे समूह नष्ट हो जाते हैं । साथ ही उसका प्राण व मन ब्रह्मा ( परमात्मा ) में संयुक्त ( लीन ) हो जाते हैं । :- जब साधक अपने दोनों कान, दोनों आँख, नासिका के दोनों छिद्रों और मुहँ को बन्द कर लेता है । तब उसे पूरी तरह से शुद्ध सुषुम्ना मार्ग से पूरी तरह से स्पष्ट व पवित्र नाद सुनाई पड़ता है ।
शङ्खदुन्दुभिनादं च न श्रृणोति कदाचन । काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम् ।। 106 ।। भावार्थ :- उन्मनी ( समाधि ) अवस्था प्राप्त होने पर साधक का शरीर ध्रुव तारे व लकड़ी की तरह ही स्थिर हो जाता है । तब उस योगी को शंख व दुन्दुभि आदि तीव्र ध्वनि वाले नाद नहीं सुनाई देते । विशेष :- ध्रुव तारे की यह विशेषता होती है कि वह सदा एक ही जगह पर स्थिर रहता है । किसी भी परिस्थिति में वह अपनी जगह नहीं बदलता । अतः उसे स्थाई माना जाता है तभी यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया है । ठीक इसी प्रकार लकड़ी का टुकड़ा भी स्थिर होता है ।
आरम्भ अवस्था के लक्षण
सर्वावस्थाविनिर्मुक्त: सर्वचिन्ताविवर्जित: । मृतवत्तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशय: ।। 107 ।। भावार्थ :- जो योगी साधक सभी अवस्थाओं से मुक्त ( रहित ) होता है, सभी प्रकार की चिन्ताओं से जो दूर होता है । वह मरे हुए प्राणी की भाँति स्थिर रहता है । ऐसा योगी पूर्ण रूप से मुक्त होता है । इसमें किसी तरह का कोई सन्देह ( शक ) नहीं है ।
खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा । साध्यते न स केनापि योगी युक्त: समाधिना ।। 108 ।। भावार्थ :- समाधिस्थ योगी सभी प्रकार की अवस्थाओं से मुक्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता । न ही कर्म संस्कार उसको बाधा सकते हैं । ऐसे योगी को किसी भी प्रकार के उपाय से वश ( नियंत्रण ) में नहीं किया जा सकता । वह सदा मुक्त ही रहता है
न गन्धं न रसं न च स्पर्शं न नि:स्वनम् । नात्मानं न परं वेत्ति योगी युक्त: समाधिना ।। 109 ।। भावार्थ :- समाधिस्थ योगी को किसी भी प्रकार की गन्ध, रस, रूप ( दर्शन ) व स्पर्श आदि का अनुभव नहीं होता । वह इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान से रहित अवस्था वाला हो जाता है । यहाँ तक की उसे अपना व दूसरे प्राणियों का भी ध्यान नहीं रहता । वह तो पूरी तरह से मुक्त हो कर रहता है ।
चित्तं न सुप्तं नो जाग्रत् स्मृतिविस्मृतिवर्जितम् । न चास्तमेति नोदेति यस्यासौ मुक्त एव स: ।। 110 ।। भावार्थ :- जिस भी योगी साधक का चित्त जाग्रत व सुप्त अवस्था से, स्मृतियों व विस्मृतियों से व उदय और अस्त से पूरी तरह से अप्रभावित ( रहित ) है । वही साधक पूरी तरह से मुक्त अवस्था वाला होता है ।
न विजानाति शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा । न मानं नापमानं च योगी युक्त: समाधिना ।। 111 ।। भावार्थ :- समाधिस्थ योगी को कभी भी सर्दी- गर्मी, सुख- दुःख व मान- अपमान का अनुभव नहीं होता । वह इन सभी द्वन्द्वों से पूरी तरह से मुक्त होता है । इनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता अर्थात् वह इन सभी स्थितियों में सम रहता है ।
स्वस्थो जाग्रदवस्थायां सुप्तवद्योऽवतिष्ठते । नि:श्वासोच्छ् वासहीनश्च निश्चितं मुक्त: एव स: ।। 112 ।। भावार्थ :- जो योगी साधक पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है । वह जागते हुए भी सोये हुए के समान स्थिर रहता है अर्थात् उसमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं रहती । उसके श्वास व प्रश्वास की गति भी स्थिर ( नियन्त्रित ) हो जाती है । इसी अवस्था वाला साधक ही निश्चित रूप से मुक्त होता हैं ।
अवध्य: सर्वशस्त्राणामशक्य: सर्वदेहिनाम् । अग्राह्यो मन्त्रयन्त्रणां योगी युक्त: समाधिना ।। 113 ।। भावार्थ :- समाधिस्थ योगी का शरीर सभी प्रकार के हथियारों के प्रभाव से रहित होता है अर्थात् उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र से मारा नहीं जा सकता । साथ ही वह सभी प्राणियों के नियंत्रण से बाहर होता है । उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई तन्त्र- मन्त्र की शक्ति भी असर नहीं करती है । इस प्रकार वह योगी अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण होता है ।
यावन्नैव प्रविशति चरन् मारुतौ मध्यमार्गे यावद् बिन्दुर्न भवति दृढ: प्राणावातप्रबन्धात् । यावद् ध्याने सहजसदृशं जायते नैव तत्त्वम् तावज्ज्ञानं वदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलाप: ।। 114 ।। भावार्थ :- जब तक साधक का चलता हुआ प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं करता है, जब तक प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा वीर्य शरीर में स्थिर नहीं होता, जब तक उस परमतत्त्व ( परमात्मा ) का ध्यान आसानी से नहीं हो जाता । तब तक उसे जो ज्ञान है अर्थात् जिसे वह ज्ञान मानता है । वह अभिमान द्वारा पैदा हुआ झूठा राग ही है ।
Last Date Modified
2024-11-23 15:51:30Your IP Address
216.73.216.24
Your Your Country

Total Visitars
14Powered by Triveni Yoga Foundation
Last Date Modified
2024-11-23 15:51:30Your IP Address
216.73.216.24
Your Your Country

Total Visitars
14Powered by Triveni Yoga Foundation

Powered by Triveni Yoga Foundation